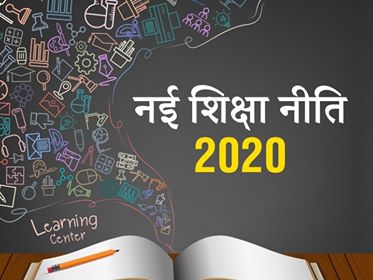भारतीयता की महान विरासत से युक्त, महात्मा गाँधी के विजन से अनुप्राणित, डॉ. आम्बेडकर के दिए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है. देर आयद पर दुरुस्त आयद इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में एक ओर जहाँ शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान खामियों को दूर करने के प्रावधान हैं, तो दूसरी ओर 21वीं सदी के बदलते हुए भारत की आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों का सामने करने की तैयारी भी.
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की एक बड़ी विशेषता है कि यह सच्चे मायने में एक राष्ट्रीय नीति है. दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की चारों दिशाओं से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 676 जिलों के शिक्षकों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, अभिभावकों और छात्रों से सुझाव और मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप यह एनईपी साकार हुई है. इस रूप में यह एक लोकतांत्रिक रीति से तैयार हुई शिक्षा नीति है.
एक अन्य नया परिवर्तन है कि एनईपी 2020 की घोषणा साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर ‘शिक्षा मंत्रालय’ कर दिया गया है, जो सर्वथा उचित है. ‘मानव संसाधन’ से ध्वनित होता है कि मानवीय भावों-संस्कारों से रहित इंसान जैसे एक भौतिक संसाधन मात्र हो, जो पश्चिम के भौतिकवादी चिन्तन से प्रेरित है. जबकि ‘शिक्षा’ अभिधान मनुष्य के भौतिकवादी पहलु के साथ-साथ सांस्कृतिक, चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक सभी पक्षों को समाहित करता है, जो भारतीय चिंतन-पद्धति का प्रतिबिम्बन है.
भारतीय भाषाओँ पर जोर एनईपी की एक बड़ी विशेषता है. स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में ‘भारतीय भाषाओँ के अध्यापन’ के साथ- साथ ‘भारतीय भाषाओँ में अध्यापन’ पर बल दिया गया है. एक महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाँचवी ग्रेड तक की पढ़ाई होगी, जिसे आठवीं तक भी बढ़ाया जा सकता है. अंग्रेजी होगी अब भी, लेकिन अब सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी. यूनेस्को रिपोर्ट अथवा शैक्षणिक मनोविज्ञान के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता है क्योंकि इसमें सम्प्रेषण व संज्ञान सहज व शीघ्र होता है. मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चा समझता है जबकि इतर भाषाओँ में उसे रटना पड़ता है. यह अनायास नहीं कि संसार के हर विकसित देश में स्कूली शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही होती है. यहाँ तक की उच्च शिक्षा का माध्यम भी सामान्यतया उनके देश की भाषा होती है. एनईपी का यह बिंदु भारतीय भाषाओँ और संस्कृति दोनों ही की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
एनईपी का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है ‘सबका साथ, सबका विकास’ को साकार करने के लिए ‘सबको शिक्षा’ देने की महत्वकांक्षी योजना. इसमें ‘राइट टू एजुकेशन’ को 14 साल से आगे बढ़ाकर 100% जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर तक ‘एजुकेशन फ़ॉर ऑल’ का लक्ष्य रखा गया है. सन 2030 तक 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क होगी. यही नहीं हमारे युवाओं की ऊर्जा का उचित उपयोग हो, इसके लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी. यही नहीं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े इसके लिए 2030 तक लगभग हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक वृहत उच्च शिक्षा संस्थान होगा.
सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े- वंचित तबकों के लिए भी एनईपी सजग है. एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों और गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएँगे. महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इनके लिए निशुल्क शिक्षा या छात्रवृति के लिए प्रयास किए जाएँगे. निजी संस्थानों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए एक कैपिंग (capping) भी होगी. निजी एचईआई द्वारा निर्धारित सभी शुल्क पारदर्शी होंगे. सार्वजानिक या निजी सभी शिक्षा संस्थानों को ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों निर्धारित किए जाएँगे.
वर्तमान के मैकाले मॉडल पर आधारित शिक्षा किताबी ज्ञान व शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर जोर देती है, जो पढ़ाई के बाद नौकरी ढूँढने वाले बेरोजगारों की बड़ी खेप तैयार कर रही है. लेकिन एनईपी पाठ्येतर क्रियाकलापों और वोकेशनल शिक्षा पर भी बल देती है. महात्मा गांधी के श्रम-सिद्धांत के अनुरूप छठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसमें ‘कोडिंग’ जैसे आधुनिकतम वोकेशनल प्रशिक्षण भी शामिल होंगे. अच्छी बात यह है कि कॉलेज स्तर पर भी वोकेशनल प्रशिक्षण के विभिन्न कोर्सेस उपलब्ध होंगे. अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्यापन के दौरान मैंने देखा कि उनके करिकुलम में वोकेशनल शिक्षा का घटक जरूर होता है. नए मॉडल में रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
एनईपी की एक अन्य विशेषता है कि शिक्षा में स्ट्रीम की खांचेबंदी नहीं होगी. अब साइंस या कॉमर्स का छात्र आर्ट्स और सोशल साइंस के विषय भी पढ़ सकेगा. महत्वपूर्ण है कि यह लचीलापन माध्यमिक स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन में भी होगा. यूरोप- अमेरिका आदि में बहुत पहले से मौजूद यह पैटर्न एक अंतर्विषयक दृष्टि पैदा करेगी, जो मल्टी-टास्किंग और भावी इंटिग्रेटेड रिसर्च के लिए उपयोगी होगा. मल्टी-एंट्री और मल्टी-एग्जिट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की एक नई विशेषता होगी. अभी तीन वर्षीय ग्रेजुएशन में यदि छात्र को किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़े तो सारा परिश्रम, धन तथा समय बेकार चला जाता है. अब एक साल अथवा दो साल में भी पढ़ाई छोड़ने पर उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरुर मिलेगा. बल्कि एक तय सीमा में वापस आकर वह अपनी बची पढाई पूरा कर सकता है. ‘एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स’ एनईपी का एक अन्य क्रांतिकारी प्रावधान है. यह एक डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा, जिसके द्वारा किसी एक संस्थान या प्रोग्राम में प्राप्त क्रेडिट को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा. किन्हीं मज़बूरी में संस्थान या शहर बदलने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत आश्वस्तकारी है.
यह सर्वविदित है कि किसी राष्ट्र की प्रगति में शोध-अनुसंधान की बड़ी भूमिका होती है. इसीलिए मोदी सरकार, अटल सरकार के ‘जय विज्ञान’ से आगे जाकर ‘जय अनुसंधान’ को एनईपी में बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध दिखती है. देश में एक मज़बूत शोध-अनुसंधान संस्कृति तथा क्षमता विकसित हो, इसके लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (एनआरएफ़) की स्थापना का प्रावधान है. उच्च शिक्षा में एकीकृत एवं समन्वित नीति व लक्ष्य निर्धारण हेतु विभिन्न निकायों का विलय करके एक सिंगल रेगुलेटर ‘भारत उच्च शिक्षा आयोग’ (एचईसीआई) का गठन एनईपी का एक अन्य अहम बिंदु है.
समग्रता में देखें तो लोकल से लेकर ग्लोबल, भारत केंद्रितकता से लेकर वैश्विकता, रोजगार से लेकर अनुसंधान और चरित्र निर्माण से लेकर भौतिक उपलब्धि— सभी दृष्टियों से उच्च लक्ष्यों वाली एनईपी 21वीं सदी में भारत की जरूरतों-चुनौतियों को पूरा करने की दिशा में एक दूरदर्शी विजन डॉक्युमेंट है. इसका क्रियान्वयन एक चुनौती जरूर होगी, लेकिन अगर योग्य लोगों को इसमें शामिल किया जाए तो इसे हासिल करना कठिन नहीं होगा.
(लेखक दिल्ली विवि के हिन्दी विभाग में प्रोफेसर हैं, और पूर्व में कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुके हैं l यह उनके निजी विचार है l)
छवि स्रोत: https://static.abplive.com
(The views expressed are the author's own and do not necessarily reflect the position of the organisation)